

उदारा: सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् |
आस्थित: स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् || 18||
उदारा:-महान; सर्वे सभी; एव–वास्तव में; एते-ये; ज्ञानी–वे जो ज्ञान में स्थित रहते हैं; तु–लेकिनः आत्मा-एव-मेरे समान ही; मे मेरे; मतम्-विचार; आस्थित:-स्थित; सः-वह; हि-निश्चय ही; युक्त-आत्मा भगवान में एकीकृत; माम्-मुझे एव–निश्चय ही; अनुत्तमाम्-सर्वोच्च गतिम्-लक्ष्य।
BG 7.18: वास्तव में वे सब जो मेरे प्रति शरणागत हैं, निःसंदेह महान हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझमें विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ।
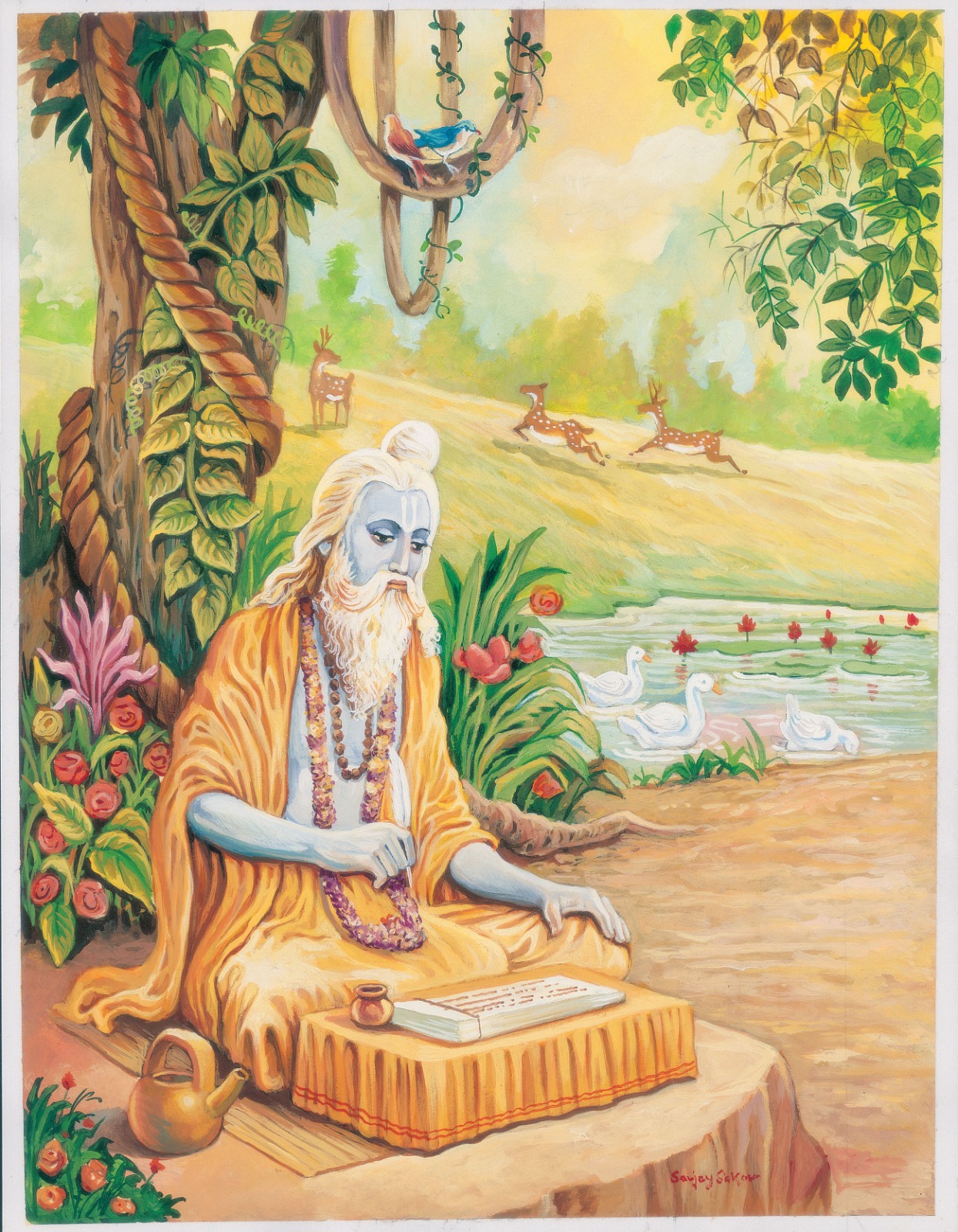
Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!
श्लोक 7.17 में ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताने के पश्चात् श्रीकृष्ण अब स्पष्ट करते हैं कि अन्य तीन प्रकार के भक्त भी पुण्यात्मा हैं। जो मनुष्य किसी भी कारण से भक्ति में लीन रहते हैं, वे भी सौभाग्यशाली हैं। फिर भी वे भक्त जो ज्ञान में स्थित होते हैं, वे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भगवान की भक्ति नहीं करते। जिसके परिणामस्वरूप भगवान ऐसे भक्तों के निष्काम और निश्छल प्रेम में बँध जाते हैं। पराभक्ति या दिव्य प्रेम सांसारिक प्रेम से अत्यंत भिन्न होता है। यह परम प्रियतम के सुख की भावना से ओत-प्रोत होता है जबकि सांसरिक प्रेम आत्म सुख की इच्छा से प्रेरित होता है। दिव्य प्रेम देने और अपने प्रियतम की सेवा के लिए प्रेयसी के त्याग की भावना से युक्त होता है किन्तु संसारिक प्रेम में लेने की भावना प्रधान होती है। सांसारिक प्रेम में लेने की प्रवृत्ति ही चित्रित होती है जिसमें प्रियतम से कुछ प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य होता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से वर्णन किया है
कामेर तात्पर्य निज-सम्भोग केवल ।
कृष्ण-सुख-तात्पर्य-मात्र प्रेम त' प्रबल ।।
अतएव काम-प्रेमे बहुत अन्तर ।
काम अन्ध-तम प्रेम निर्मल भास्कर ।।
(चैतन्य चरितामृत आदि लीला-4.166-167)
"काम-वासना आत्म सुख के लिए होती है, किन्तु दिव्य प्रेम में मन श्रीकृष्ण के सुख में ओत-प्रोत रहता है। इन दोनों में असाधारण भिन्नता पायी जाती है। काम वासना अज्ञान के अंधकार के समान है जबकि दिव्यप्रेम शुद्ध और प्रकाशमय सूर्य के समान होता है।" ।
जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे अत्यंत सुन्दरता से व्यक्त किया है
ब्रह्मलोक पर्यंत सुख, अरु मुक्तिहुँ सुख त्याग।
तबै धरहु पग प्रेम पथ, नहिं लगि जैहैं दाग।।
(भक्ति शतक-45)
"यदि तुम भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हो तब सांसारिक सुखों और मुक्ति की कामनाओं का त्याग कर दो। अन्यथा दिव्यप्रेम का शुद्ध जल स्वार्थ रुपी मल से दूषित हो जाएगा।" नारद मुनि ने विशुद्ध भक्ति का निरूपण इस प्रकार से किया है
तत्सुख्सुखित्वम् ।।
(नारद भक्ति दर्शन, सूत्र-24)
"सच्चा प्यार प्रियतम के सुख के लिए होता है।" सांसारिकता द्वारा अभिप्रेरित भक्त ऐसी भक्ति में लीन नहीं हो सकते लेकिन जिस भक्त को इसका ज्ञान होता है वह निजी स्वार्थ के स्तर से ऊपर उठ जाता है। जब कोई इस प्रकार से भगवान से प्रेम करना सीख जाता है तब भगवान उस भक्त के दास बन जाते हैं। भगवान का सबसे बड़ा गुण भक्तवत्सलता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख किया गया है
गीत्वा च मम नामानि विचरेन्मम सन्निधौ।
इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोहं तस्य चार्जुन ।।
(आदि पुराण-1.2.231)
श्रीकृष्ण कहते हैं "मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूँ जो मेरे नामों की महिमा का गान करते हैं और अपने ध्यान में मेरा ही चिन्तन करते हैं। हे अर्जुन! यह सत्य है-भगवान अपने निष्काम परमभक्तों के ऋणी हो जाते हैं।" गीता के इस श्लोक में तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि वे ऐसे भक्तों को अपने समान देखते हैं।